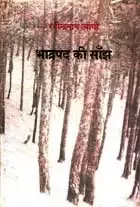|
हास्य-व्यंग्य >> भाद्रपद की साँझ भाद्रपद की साँझरवीन्द्रनाथ त्यागी
|
165 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है हास्य-व्यंग्य संग्रह...
Bhadrapad ki sanjh a hindi book by Ravindranath Tyagi - भाद्रपद की साँझ - रवीन्द्रनाथ त्यागी
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
रवीन्द्रनाथ त्यागी ने न तो शुद्ध हास्य लिखा, न शुद्ध व्यंग्य और न शुद्ध ललित-निबंध। तीनों की मिली-जुली विशेषताओं को लेकर उन्होंने अपने खास रंग को शोख़ व चटख़ बनाया। उनके लेखन से जो आनन्द मिलता है, वह इधर के बहुत सारे लेखन से नहीं मिलता। जो लेखन एक ‘ज्वॉय’ दे, एक ‘एक्सटेसी’ दे, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे भी जितना वैविध्य रवीन्द्रनाथ त्यागी में है, उतना उनके समकालीन किसी भी व्यंग्यकार के पास नहीं है....
डॉ.धनंजय वर्मा
रवीन्द्रनाथ त्यागी को पढ़ना मुश्किल है क्योंकि बीच-बीच में हँसना पड़ता है। मुझे हँसते देखकर घर के सयाने बच्चे और विद्वान अनुसंधित्सु मेरी हँसी उड़ाते हैं और पुस्तक को मेरे हाथ से छीनकर पढ़ने लगते हैं। जब वे भी हँसने लगते हैं तो मैं इस शून्यकाल का फायदा उठाकर पुस्तक फिर पढ़ने लगता हूँ। त्यागीजी की भाषा नटखट, प्रभावशाली व सुखकारी है। मैं उनके साहित्य को व्यंजना-कौशल की बारीकियों की दृष्टि से ‘व्यंग्य’ कहता हूँ। उन्होंने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया है और बहुमुखी संदर्भशीलता भी उनके साहित्य में हैं। व्यंग्य का ‘मूलतत्त्व’ है भाषा में अभिव्यंजना की एक विशेष शक्ति पैदा करना। रवीन्द्रनाथ त्यागी तथा श्रीलाल शुक्ल के अतिरिक्त किसी और हिन्दी व्यंग्यकार के पास अध्ययन-गर्भित प्रजातीय संस्कृति की भाषा-संश्लिष्टता और बहुविद्या के साथ-साथ शब्द-मुद्रा में विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हुए कथन-काकु के द्वारा व्यंग्य उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है...
डॉ.शुकदेव सिंह
रवीन्द्रनाथ त्यागी का गद्य मुझे अच्छा ही नहीं वरन् बहुत अच्छा लगता है। उनके लेखन में व्यंग्य व लालित्य-दोनों हैं। उनके अनुभव का आयाम बहुत विस्तृत है। मैं तो चाहता हूँ कि इसी शैली में वे अपनी आत्मकथा लिखें......
डॉ.कुबेरनाथ राय
धूप के धान
देहरादून सचमुच एक रूपवती नगरी है। यूँ तो यहाँ नीले पर्वतों की श्रेणियाँ हैं, गहरे हरे रंग के घने वनों से ढके क्षितिज हैं, पग-पग पर धोखा देनेवाले रंग-बिरंगी सड़के हैं और धान के पीले-पीले खेतों से ढकी घाटियाँ हैं। पर यहाँ का प्रमुख आकर्षण जो है वह यहाँ कि वर्षा ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में (जिसका काफ़ी भाग देहरादून की जिला-जेल में ही लिखा गया था) स्वीकार किया है कि देहरादून सचमुच वर्षा के राजा इंद्र की सर्वप्रिय नगरी है। वर्षा की पवित्र ऋतु यहाँ प्रायः बारह महीने चलती है और फिर जो वर्ष का शेष भाग बचता है उसमें शेष सारी ऋतुएँ प्रकट होती हैं और काफ़ी ज़िम्मेदारी से अपना-अपना काम करती हैं। वर्षा शुरू होती है
तो सचमुच बेहद सुंदर लगती है और आपको ‘बादल घिर आए, गीत की बेला आई’ जैसी मार्मिक पंक्तियाँ याद आने लगती हैं। मगर जब यही वर्षा ज़्यादा खिंच जाती है तो आपको अपने आप पता लगने लगता है कि वर्षा के दिन को ‘दुर्दिन’ क्यों कहते हैं। टेलीफ़ोन ख़राब हो जाता है। बिजली भाग जाती है
और अख़बार और डाक का आना भी बंद हो जाता है। प्रियाहीन न होते हुए भी मेरा मन डरने लगता है और मेघदूत को खड्ड की दिशा में फेंकने की पवित्र प्रवृत्ति फिर ज़ोर पकड़ने लगती है। वर्षा में मुझे सबसे ज़्यादा डर दीमक नामक कीड़े से लगता है जिसकी संतति ‘चंद्रकांता-संतति’ से भी ज़्यादा होनहार होती है और जिसके दर्शन कर मुझ जैसे भूतनाथ को भी अभूतपूर्व भय लगने लगता है। वैसे मैंने अपने जीवन में सदा ही प्रत्येक आकर्षण रमणी को एक तिलस्म ही समझा और मेरा यह विश्वास प्रायः ठीक ही निकला। रमणी शायद मुझे छोड़ दे पर मेरी किताबें कभी नहीं छोड़ेगी।
वर्षा थमने के बाद धूप का निकलना प्रायः उतना ही निश्चित होता है जितना कि प्रत्येक कन्या का अपने विवाह के बाद गर्भवती होना होता है। बादलों के फटने पर जो धूप निकलती है वह उबटन लगी किसी गौरवर्णा युवती के अंगों की भाँति एकदम निखरी हुई होती है। धूप यह जादू आपको न जाने कितने कवियों की वाणी को एक साथ याद दिलाने लगता है। पंतजी ने ऐसी ही धूप में लेटने के बाद कहा होगा कि ‘सोने के तार-सा खिंच गया है दिन’ और गिरिजाकुमार माथुर ने जो ‘धूप के धान’ बोए या काटे थे वे भी किसी ऐसे ही दिन बोए या काटे होंगे। ‘धान’ से प्रेम बाकी कवियों को भी रहा
और ‘धूप’ से कहीं ज्यादा रहा। ‘सुजलां सुफलां मलयज शीतलां’ कहने के बाद ‘शस्य श्यामलां कहनेवाले और आनंदपूर्वक किसी मठ में बिराजनेवाले ‘गर्दभ-स्तोत्र’ के कवि बंकिमचन्द्र से लेकर ‘‘स्वर्ण-शस्य अंचल धरती का लहराया’’ कहने वाले ‘निराला’ तक ‘कनक-शस्य’ के कवि नरेन्द्र शर्मा से लेकर ‘‘हम जिए न जिए दोस्त / तुम जिओ एक नौजवान की तरह/ खेत में झूम रहे धान की तरह’’ लिखनेवाले केदारनाथ अग्रवाल जैसे सभी सौंदर्यवादी कवि वर्षा में भी धान की दूकान के ही बाहर लाइन लगाकर खड़े रहे और भीगते रहे। हाँ,
अज्ञेय ने एक बार अपनी एक प्रेयसी की तुलना ज़रूर बाजरे की कलगी से की और अपने एक गीत में ‘निराला’ ने भी मूँग और उड़द की चर्चा की।‘ कनक कनक ते सौ गुनी’ कहनेवाले बिहार के महाकवि बिहारीलाल ने अपना या अपनी प्रेयसी का स्तर कभी भी गेहूँ के नीचे आने नहीं दिया। ठाकुर प्रसाद सिंह ने ‘‘कचमच धूप, हवाएँ सन सन/ आछी के वन’’ कहकर धूप का जितना बढ़िया ख़ाका खींचा उतना ही विचित्र वर्णन धूप का केदारनाथ अग्रवाल ने तब किया जब उन्होंने लिखा कि ‘‘धूप नहीं वह/ बैठा है खरगोश पलंग पर / जिसको छूकर / ज्ञान हुआ मुझको / जीने का।’’ अब यह भी कोई बात हुई कि एक अदद ख़रगोश है जो पलंग पर बैठा है और कविजी है
ं जो उसे देख-देखकर जल्दी-जल्दी कविता लिख रहे हैं क्योंकि ख़रगोश बड़ा पाजी जानवर होता है और इसका कुछ पता नहीं कि कवि की कविता को बीच में ही छोड़कर कब अंतर्धान हो जाए। अरे ओ मेरे कवि बंधु, पलंग पर बिठाना ही था तो किसी काम की चीज को बिठाते जिससे की पलंग की शोभा बढ़ती। ख़रगोश को वहां बिठाने पर तुम्हें या ख़रगोश को क्या मिला ? तुमसे श्रेष्ठ तो देहरादून के वे कवि हैं जो बराबर बासमती ‘चावल’ पर ही कविता लिखते हैं और इसी कारण ‘चावला’ कहलाते हैं।
वर्षा के बाद धूप बिखर गई। अब डाकिए की प्रतीक्षा करूँगा हालाँकि वह बिजली या टेलीफ़ोन (या दोनों) का बिल ही लाएगा, और कुछ नहीं।
मेरे बरामदे में पर्वतों की नीली श्रेणियाँ अब चमकेंगी। मित्र आएँगे विभिन्न साइज़ों की गप्पे मारी जाएँगी और ‘निराला’ की बहुत दिनों बाद खुला आसमान, खुश हुआ जहान’’ पंक्तियोंवाली कविता फिर पढ़ी जाएगी। इसी कविता में आगे चलकर नयनों के बाण चलानेवाली चंद हसीन ग्राम बालाओं की चर्चा की गई है और थोड़ा-सा वर्णन कुछ ‘तगड़े-तगड़े पहलवानों’ का भी किया गया है। श्रृंगार का जो अद्वितीय संगम ‘निराला’ के कृतित्व में है,
वैसा शायद और कहीं नहीं है। और निरालाजी स्वयं भी तो एक पहलवान थे जिन्होंने एक बार पंतजी को भी कुश्ती के लिए ललकारा था। ‘कुश्ती’ का पुल्लिंग ‘कुश्ता’ होता है। शहंशाह शाहजहाँ की मृत्यु जो हुई थी वह कुश्ता खाने के कारण ही हुई थी। उनकी प्रिय बेगम मुमताजमहल चौदह वर्ष तक लगातार गर्भवती रही थी।
इस दमकती हुई धूप को देखकर मुझे मेघदूत की याद फिर सताने लगी जिसके रूप का वर्णन कालिदास ने ‘‘तन्वी, श्यामा, शिखरदशना, पक्वबिम्बाधरोष्ठी’’ कहकर शुरू किया। इस पंक्ति में जो ‘श्यामा’ शब्द है उसका सही अर्थ जानने में मेरी आधी उम्र निकल गई। ‘श्यामा’ का प्रत्यक्ष अर्थ ‘साँवली’ या ‘कृष्णवर्णा, हो सकता था पर कालिदास जैसा रससिद्ध कवि अपनी प्रिय नायिका को उस रूप में देख सकता था ?
उसे क्या गौरवर्णा रमणियों की कोई कमी थी ? मैंने राजा लक्ष्मणसिंह से लेकर बाबू श्यामसुंदर दास (बी.ए.) तक जितने भी बड़े-बड़े विद्वानों के अनुवाद हैं, वे सब देखे। सबमें से ‘श्यामा’ शब्द का सही अर्थ कोई भी पंडित नहीं जानता था। कुछ ने तो ‘श्यामा’ का अनुवाद ‘श्यामा’ ही किया है और कुछ मतिमान् लोगों ने अपने अनुवाद में श्यामा’ का जिक्र ही नहीं किया है। बहुत दिनों बाद मैत्रेयी देवी की टैगोर बाई फ़ायरसाइड नामक श्रेष्ठ पोथी पढ़ने को प्राप्त हुई और उसमें रवींद्रनाथ ठाकुर की वाणी पढ़ने को मिली जिसमें यह बताया गया है कि संस्कृत में ‘श्यामा का अर्थ उस स्त्री से है जिसका कि रंग उस, स्वर्ण की भाँति दमकता है
जो कि प्रज्जवलित अग्नि में पिघलता जा रहा हो। इसी प्रकार गीता के अठारहवें अध्याय के चौदहवें श्लोक में ‘दैव’ शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का भी अर्थ जानने के लिए मैं बहुत भटका मगर सब दिशाओं में निराशा ही हाथ लगी। अंत में चलकर लोकमान्य तिलक की प्रख्यात पुस्तक गीता-रहस्य की शरण में गया मगर मैंने पाया कि तिलक जैसे महान् ज्ञानी पुरुष ने भी ‘दैव का अर्थ ‘दैव’ ही लिखा है, और कुछ नहीं। [मेरे पास इस पुस्तक का सप्तम संस्करण है जिसके प्रारंभ में बताया गया है कि लोकमान्य तिलक के पुत्रों के साथ कोई भंयकर मुक़द्दमेबाज़ी चली थी जिसके फलस्वरूप इन पुत्रों में से एक ज्ञानी पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी।
पिता द्वारा किए गीता के भाष्य का पुत्रों पर ऐसा तात्कालिक प्रभाव पड़ेगा यह कोई नहीं जानता था।] मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा भी दमकते स्वर्ण जैसा ही वर्ण रखती थी। यदि वैसी न होती तो आप ही बताइए कि वह पवित्र रमणी अपने छोटे से क्षणभंगुर जीवन काल में दस हज़ार प्रेमियों की हम-बिस्तर कैसे हो सकती थी ? इतिहासकारों का कहना है कि क्लियोपेट्रा की नाक अगर और लंबी होती तो विश्व का इतिहास कुछ और ही होता। इस सम्राज्ञी के दस हज़ार प्रेमियों में रोम का महान् सम्राट् जूलियस सीज़र बाक़ायदा शामिल था।
विलियम शेक्सपीयर ने इस सारी घटना का अत्यंत संक्षिप्त वर्णन करते हुए मात्र इतना ही लिखा है कि ‘‘क्लियोपेट्रा सीज़र को तलवार से हटाकर पलंग पर ले गई।’’ इस परम पवित्र घटना के समय सम्राट जूलियस सीज़र क्लियोपेट्रा से उम्र में मात्र तीस वर्ष बड़ा था। बारह वर्ष की आयु में ही अपना कौमार्य भंग करने वाली रूपसी क्लियोप्रेट्रा मात्र इक्कीस वर्ष की कन्या थी और जूलियस सीज़र इक्यावन वर्ष का अधेड़ था। सादा जीवन, उच्च विचार।
अब मैं क्लियोपेट्रा को सम्राट् जूलियस सीज़र के हवाले करता हूं और फिर उसी धूप को कसकर पकड़ता हूँ जिसे मैंने किसी भूतपूर्व प्रेमिका की भाँति बीच में ही छोड़ दिया था। जैसे देश में उपराष्ट्रपति व उपराष्ट्रकवि होते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे बंगले में एक उपवन है। धूप निकलने पर उसमें विचरण करने में जो सुख मिलता है वह मुझे कभी अपने किसी उप-पत्नी के साथ भी नहीं मिला। इस वाटिका में मालती की लता है,
केले के गाछ की छटा है और शेष जो विभिन्न प्रकार के वृक्ष या उपवृक्ष हैं, उनकी भी घटा है। यूकलिप्टस, चीड़, सिल्वर ओक, पापलर जैसे पहाड़ी वृक्षों के साथ-साथ शीशम आम, जामुन, अमरूद, लीची, नाशपाती और अनार जैसे मैदानी वृक्ष भी खुशी-खुशी खड़े हैं और कलावती नाम की कन्या की भाँति यौवन को प्राप्त कर रहें हैं। देहरादून की जलवायु ऐसी है कि यहाँ फलवाले वृक्षों पर भी फल कम और पत्ते ज्यादा आते हैं।
एक बड़ा वृक्ष ‘फ़ज़री’ आम का है हालाँकि हम सब लोग उसे ‘लँगड़ा आम कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर चढ़कर चोरी से आम तोड़ने की प्रक्रिया में आसपास के कई संभ्रांत किशोर लँगड़े हो चुके हैं। पारसी थियेटर के बादशाह आग़ा हश्र कश्मीरी को उनके एक शरारती मित्र ने एक बार ‘बनारस का लँगड़ा’ कह दिया था क्योंकि आग़ा ख़ां साहब बनारस के ही थे और वे थोड़े-से लँगड़े भी थे।
बनारस का शहर सदियों में राँड-साँड, सीढ़ी, संन्यासी, लँगड़ा आम, साड़ियाँ और जर्दे के लिए मशहूर रहा। बाद में चलकर यह नगर भारतेंदु हरिशचंद्र, देवकीनंदन खत्री, मुशी प्रेमचंद्र, बाबू श्यामसुंदर दास, जयशंकर ‘प्रसाद’, रामचंद्र शुक्ल व आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के कारण भी प्रसिद्ध रहा पर ये सारे विद्वान् भी वहाँ के साँड और ज़र्दे वग़ैरा का स्तर नहीं छू पाए।
सारे ‘उत्तरप्रदेश’ में व ‘हाथरस’ के अतिरिक्त और कोई ‘सरस’ नगर है ही नहीं। बाकी सब नगर तो मात्र ‘नीरस’ हैं। बिसमिल्ला ख़ाँ की वह शहनाई और हाथरस की वह ‘खुरचन’ और कहाँ मिलेगी ?’’
उपवन में भ्रमण करने के पश्चात् मैंने मिस्त्री को तलब किया जिसने लगभग मात्र दस वर्ष पूर्व मेरा यह बँगला बनाया था जो प्रत्येक वर्षा में काफ़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ चूता है। मिस्त्री साहिब तशरीफ़ लाए और अंदर और बाहर का मुकम्मल मुआयना करने के बाद कॉफी और सिगार पीते हुए कहने लगे कि बँगले के चूने का एकमात्र कारण यह है कि बँगला अभी नया है और यह इसी कारण चूता है।
मैं इन मिस्त्री महोदय को भली-भाँति जानता हूँ और मुझे पता है कि पाँच वर्ष बाद ये अपना मौजूदा अंदाज़ बदल देंगे और कहा करेंगे कि अब बँगला इस कारण चूता है क्योंकि अब पुराना होने लगा है। आदमी बड़े दिलचस्प हैं। एक दफा मैंने इनकी कुशलता के बारे में कुछ संशय प्रकट किया तो कहने लगे कि आगरे का ‘मक़बरा ताजमहल’ और बंबई का ‘होटल’ ताजमहल’ इन्हीं के बुजुर्गों ने एक साथ ही बनाया था।
तो सचमुच बेहद सुंदर लगती है और आपको ‘बादल घिर आए, गीत की बेला आई’ जैसी मार्मिक पंक्तियाँ याद आने लगती हैं। मगर जब यही वर्षा ज़्यादा खिंच जाती है तो आपको अपने आप पता लगने लगता है कि वर्षा के दिन को ‘दुर्दिन’ क्यों कहते हैं। टेलीफ़ोन ख़राब हो जाता है। बिजली भाग जाती है
और अख़बार और डाक का आना भी बंद हो जाता है। प्रियाहीन न होते हुए भी मेरा मन डरने लगता है और मेघदूत को खड्ड की दिशा में फेंकने की पवित्र प्रवृत्ति फिर ज़ोर पकड़ने लगती है। वर्षा में मुझे सबसे ज़्यादा डर दीमक नामक कीड़े से लगता है जिसकी संतति ‘चंद्रकांता-संतति’ से भी ज़्यादा होनहार होती है और जिसके दर्शन कर मुझ जैसे भूतनाथ को भी अभूतपूर्व भय लगने लगता है। वैसे मैंने अपने जीवन में सदा ही प्रत्येक आकर्षण रमणी को एक तिलस्म ही समझा और मेरा यह विश्वास प्रायः ठीक ही निकला। रमणी शायद मुझे छोड़ दे पर मेरी किताबें कभी नहीं छोड़ेगी।
वर्षा थमने के बाद धूप का निकलना प्रायः उतना ही निश्चित होता है जितना कि प्रत्येक कन्या का अपने विवाह के बाद गर्भवती होना होता है। बादलों के फटने पर जो धूप निकलती है वह उबटन लगी किसी गौरवर्णा युवती के अंगों की भाँति एकदम निखरी हुई होती है। धूप यह जादू आपको न जाने कितने कवियों की वाणी को एक साथ याद दिलाने लगता है। पंतजी ने ऐसी ही धूप में लेटने के बाद कहा होगा कि ‘सोने के तार-सा खिंच गया है दिन’ और गिरिजाकुमार माथुर ने जो ‘धूप के धान’ बोए या काटे थे वे भी किसी ऐसे ही दिन बोए या काटे होंगे। ‘धान’ से प्रेम बाकी कवियों को भी रहा
और ‘धूप’ से कहीं ज्यादा रहा। ‘सुजलां सुफलां मलयज शीतलां’ कहने के बाद ‘शस्य श्यामलां कहनेवाले और आनंदपूर्वक किसी मठ में बिराजनेवाले ‘गर्दभ-स्तोत्र’ के कवि बंकिमचन्द्र से लेकर ‘‘स्वर्ण-शस्य अंचल धरती का लहराया’’ कहने वाले ‘निराला’ तक ‘कनक-शस्य’ के कवि नरेन्द्र शर्मा से लेकर ‘‘हम जिए न जिए दोस्त / तुम जिओ एक नौजवान की तरह/ खेत में झूम रहे धान की तरह’’ लिखनेवाले केदारनाथ अग्रवाल जैसे सभी सौंदर्यवादी कवि वर्षा में भी धान की दूकान के ही बाहर लाइन लगाकर खड़े रहे और भीगते रहे। हाँ,
अज्ञेय ने एक बार अपनी एक प्रेयसी की तुलना ज़रूर बाजरे की कलगी से की और अपने एक गीत में ‘निराला’ ने भी मूँग और उड़द की चर्चा की।‘ कनक कनक ते सौ गुनी’ कहनेवाले बिहार के महाकवि बिहारीलाल ने अपना या अपनी प्रेयसी का स्तर कभी भी गेहूँ के नीचे आने नहीं दिया। ठाकुर प्रसाद सिंह ने ‘‘कचमच धूप, हवाएँ सन सन/ आछी के वन’’ कहकर धूप का जितना बढ़िया ख़ाका खींचा उतना ही विचित्र वर्णन धूप का केदारनाथ अग्रवाल ने तब किया जब उन्होंने लिखा कि ‘‘धूप नहीं वह/ बैठा है खरगोश पलंग पर / जिसको छूकर / ज्ञान हुआ मुझको / जीने का।’’ अब यह भी कोई बात हुई कि एक अदद ख़रगोश है जो पलंग पर बैठा है और कविजी है
ं जो उसे देख-देखकर जल्दी-जल्दी कविता लिख रहे हैं क्योंकि ख़रगोश बड़ा पाजी जानवर होता है और इसका कुछ पता नहीं कि कवि की कविता को बीच में ही छोड़कर कब अंतर्धान हो जाए। अरे ओ मेरे कवि बंधु, पलंग पर बिठाना ही था तो किसी काम की चीज को बिठाते जिससे की पलंग की शोभा बढ़ती। ख़रगोश को वहां बिठाने पर तुम्हें या ख़रगोश को क्या मिला ? तुमसे श्रेष्ठ तो देहरादून के वे कवि हैं जो बराबर बासमती ‘चावल’ पर ही कविता लिखते हैं और इसी कारण ‘चावला’ कहलाते हैं।
वर्षा के बाद धूप बिखर गई। अब डाकिए की प्रतीक्षा करूँगा हालाँकि वह बिजली या टेलीफ़ोन (या दोनों) का बिल ही लाएगा, और कुछ नहीं।
मेरे बरामदे में पर्वतों की नीली श्रेणियाँ अब चमकेंगी। मित्र आएँगे विभिन्न साइज़ों की गप्पे मारी जाएँगी और ‘निराला’ की बहुत दिनों बाद खुला आसमान, खुश हुआ जहान’’ पंक्तियोंवाली कविता फिर पढ़ी जाएगी। इसी कविता में आगे चलकर नयनों के बाण चलानेवाली चंद हसीन ग्राम बालाओं की चर्चा की गई है और थोड़ा-सा वर्णन कुछ ‘तगड़े-तगड़े पहलवानों’ का भी किया गया है। श्रृंगार का जो अद्वितीय संगम ‘निराला’ के कृतित्व में है,
वैसा शायद और कहीं नहीं है। और निरालाजी स्वयं भी तो एक पहलवान थे जिन्होंने एक बार पंतजी को भी कुश्ती के लिए ललकारा था। ‘कुश्ती’ का पुल्लिंग ‘कुश्ता’ होता है। शहंशाह शाहजहाँ की मृत्यु जो हुई थी वह कुश्ता खाने के कारण ही हुई थी। उनकी प्रिय बेगम मुमताजमहल चौदह वर्ष तक लगातार गर्भवती रही थी।
इस दमकती हुई धूप को देखकर मुझे मेघदूत की याद फिर सताने लगी जिसके रूप का वर्णन कालिदास ने ‘‘तन्वी, श्यामा, शिखरदशना, पक्वबिम्बाधरोष्ठी’’ कहकर शुरू किया। इस पंक्ति में जो ‘श्यामा’ शब्द है उसका सही अर्थ जानने में मेरी आधी उम्र निकल गई। ‘श्यामा’ का प्रत्यक्ष अर्थ ‘साँवली’ या ‘कृष्णवर्णा, हो सकता था पर कालिदास जैसा रससिद्ध कवि अपनी प्रिय नायिका को उस रूप में देख सकता था ?
उसे क्या गौरवर्णा रमणियों की कोई कमी थी ? मैंने राजा लक्ष्मणसिंह से लेकर बाबू श्यामसुंदर दास (बी.ए.) तक जितने भी बड़े-बड़े विद्वानों के अनुवाद हैं, वे सब देखे। सबमें से ‘श्यामा’ शब्द का सही अर्थ कोई भी पंडित नहीं जानता था। कुछ ने तो ‘श्यामा’ का अनुवाद ‘श्यामा’ ही किया है और कुछ मतिमान् लोगों ने अपने अनुवाद में श्यामा’ का जिक्र ही नहीं किया है। बहुत दिनों बाद मैत्रेयी देवी की टैगोर बाई फ़ायरसाइड नामक श्रेष्ठ पोथी पढ़ने को प्राप्त हुई और उसमें रवींद्रनाथ ठाकुर की वाणी पढ़ने को मिली जिसमें यह बताया गया है कि संस्कृत में ‘श्यामा का अर्थ उस स्त्री से है जिसका कि रंग उस, स्वर्ण की भाँति दमकता है
जो कि प्रज्जवलित अग्नि में पिघलता जा रहा हो। इसी प्रकार गीता के अठारहवें अध्याय के चौदहवें श्लोक में ‘दैव’ शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का भी अर्थ जानने के लिए मैं बहुत भटका मगर सब दिशाओं में निराशा ही हाथ लगी। अंत में चलकर लोकमान्य तिलक की प्रख्यात पुस्तक गीता-रहस्य की शरण में गया मगर मैंने पाया कि तिलक जैसे महान् ज्ञानी पुरुष ने भी ‘दैव का अर्थ ‘दैव’ ही लिखा है, और कुछ नहीं। [मेरे पास इस पुस्तक का सप्तम संस्करण है जिसके प्रारंभ में बताया गया है कि लोकमान्य तिलक के पुत्रों के साथ कोई भंयकर मुक़द्दमेबाज़ी चली थी जिसके फलस्वरूप इन पुत्रों में से एक ज्ञानी पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी।
पिता द्वारा किए गीता के भाष्य का पुत्रों पर ऐसा तात्कालिक प्रभाव पड़ेगा यह कोई नहीं जानता था।] मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा भी दमकते स्वर्ण जैसा ही वर्ण रखती थी। यदि वैसी न होती तो आप ही बताइए कि वह पवित्र रमणी अपने छोटे से क्षणभंगुर जीवन काल में दस हज़ार प्रेमियों की हम-बिस्तर कैसे हो सकती थी ? इतिहासकारों का कहना है कि क्लियोपेट्रा की नाक अगर और लंबी होती तो विश्व का इतिहास कुछ और ही होता। इस सम्राज्ञी के दस हज़ार प्रेमियों में रोम का महान् सम्राट् जूलियस सीज़र बाक़ायदा शामिल था।
विलियम शेक्सपीयर ने इस सारी घटना का अत्यंत संक्षिप्त वर्णन करते हुए मात्र इतना ही लिखा है कि ‘‘क्लियोपेट्रा सीज़र को तलवार से हटाकर पलंग पर ले गई।’’ इस परम पवित्र घटना के समय सम्राट जूलियस सीज़र क्लियोपेट्रा से उम्र में मात्र तीस वर्ष बड़ा था। बारह वर्ष की आयु में ही अपना कौमार्य भंग करने वाली रूपसी क्लियोप्रेट्रा मात्र इक्कीस वर्ष की कन्या थी और जूलियस सीज़र इक्यावन वर्ष का अधेड़ था। सादा जीवन, उच्च विचार।
अब मैं क्लियोपेट्रा को सम्राट् जूलियस सीज़र के हवाले करता हूं और फिर उसी धूप को कसकर पकड़ता हूँ जिसे मैंने किसी भूतपूर्व प्रेमिका की भाँति बीच में ही छोड़ दिया था। जैसे देश में उपराष्ट्रपति व उपराष्ट्रकवि होते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे बंगले में एक उपवन है। धूप निकलने पर उसमें विचरण करने में जो सुख मिलता है वह मुझे कभी अपने किसी उप-पत्नी के साथ भी नहीं मिला। इस वाटिका में मालती की लता है,
केले के गाछ की छटा है और शेष जो विभिन्न प्रकार के वृक्ष या उपवृक्ष हैं, उनकी भी घटा है। यूकलिप्टस, चीड़, सिल्वर ओक, पापलर जैसे पहाड़ी वृक्षों के साथ-साथ शीशम आम, जामुन, अमरूद, लीची, नाशपाती और अनार जैसे मैदानी वृक्ष भी खुशी-खुशी खड़े हैं और कलावती नाम की कन्या की भाँति यौवन को प्राप्त कर रहें हैं। देहरादून की जलवायु ऐसी है कि यहाँ फलवाले वृक्षों पर भी फल कम और पत्ते ज्यादा आते हैं।
एक बड़ा वृक्ष ‘फ़ज़री’ आम का है हालाँकि हम सब लोग उसे ‘लँगड़ा आम कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर चढ़कर चोरी से आम तोड़ने की प्रक्रिया में आसपास के कई संभ्रांत किशोर लँगड़े हो चुके हैं। पारसी थियेटर के बादशाह आग़ा हश्र कश्मीरी को उनके एक शरारती मित्र ने एक बार ‘बनारस का लँगड़ा’ कह दिया था क्योंकि आग़ा ख़ां साहब बनारस के ही थे और वे थोड़े-से लँगड़े भी थे।
बनारस का शहर सदियों में राँड-साँड, सीढ़ी, संन्यासी, लँगड़ा आम, साड़ियाँ और जर्दे के लिए मशहूर रहा। बाद में चलकर यह नगर भारतेंदु हरिशचंद्र, देवकीनंदन खत्री, मुशी प्रेमचंद्र, बाबू श्यामसुंदर दास, जयशंकर ‘प्रसाद’, रामचंद्र शुक्ल व आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के कारण भी प्रसिद्ध रहा पर ये सारे विद्वान् भी वहाँ के साँड और ज़र्दे वग़ैरा का स्तर नहीं छू पाए।
सारे ‘उत्तरप्रदेश’ में व ‘हाथरस’ के अतिरिक्त और कोई ‘सरस’ नगर है ही नहीं। बाकी सब नगर तो मात्र ‘नीरस’ हैं। बिसमिल्ला ख़ाँ की वह शहनाई और हाथरस की वह ‘खुरचन’ और कहाँ मिलेगी ?’’
उपवन में भ्रमण करने के पश्चात् मैंने मिस्त्री को तलब किया जिसने लगभग मात्र दस वर्ष पूर्व मेरा यह बँगला बनाया था जो प्रत्येक वर्षा में काफ़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ चूता है। मिस्त्री साहिब तशरीफ़ लाए और अंदर और बाहर का मुकम्मल मुआयना करने के बाद कॉफी और सिगार पीते हुए कहने लगे कि बँगले के चूने का एकमात्र कारण यह है कि बँगला अभी नया है और यह इसी कारण चूता है।
मैं इन मिस्त्री महोदय को भली-भाँति जानता हूँ और मुझे पता है कि पाँच वर्ष बाद ये अपना मौजूदा अंदाज़ बदल देंगे और कहा करेंगे कि अब बँगला इस कारण चूता है क्योंकि अब पुराना होने लगा है। आदमी बड़े दिलचस्प हैं। एक दफा मैंने इनकी कुशलता के बारे में कुछ संशय प्रकट किया तो कहने लगे कि आगरे का ‘मक़बरा ताजमहल’ और बंबई का ‘होटल’ ताजमहल’ इन्हीं के बुजुर्गों ने एक साथ ही बनाया था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book